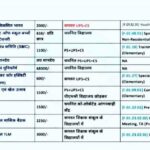आजादी के बाद से भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में कई तरह के सुधार हुए हैं, फिर भी छात्रों में सीखने का संकट बना हुआ है। बेशक शिक्षा की पहुंच बढ़ी है, लेकिन बुनियादी साक्षरता अब भी कम है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) फिर से बता रही है कि कक्षा पांच के कमोबेश आधे बच्चे दूसरी कक्षा की सरल पाठ्य सामग्री बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं। चीन ने जहां 20वीं सदी में दशकों तक प्राथमिक शिक्षा में किए गए रणनीतिक निवेश का लाभ उठाया है, वहीं भारत अब तक स्कूली शिक्षा सुधार के लिए डाटा-आधारित नजरिया नहीं अपना सका है। 2009 से चल रहे अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) जैसे वैश्विक मूल्यांकनों से दूरी भारत को उस मूल्यांकन से दूर कर देता है, जिसकी हमें जरूरत है। जाहिर है, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम को सही करने के किसी व्यवस्थित नजरिये के बिना कोई भी ढांचागत बदलाव दूर की कौड़ी साबित होगा।
सुखद बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 इन कमियों को स्वीकार करती है और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार बताए भी गए हैं। हमें यह समझना ही होगा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली, जो बुनियादी व पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर संघर्षरत हो, उस तरह के बदलाव नहीं ला सकती, जिसकी जरूरत हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में है।
इस सूरतेहाल में निजी स्कूलों की भूमिका काफी बढ़ गई है। राज्य के धीरे-धीरे पीछे हटने के साथ ही निजी संस्थानों ने इस रिक्तता को भरने का काम किया है। आज कई राज्यों में 50 फीसदी से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। हालांकि, यह क्षेत्र अब भी बंटा हुआ है, जिसके कारण नवाचार का प्रसार सीमित हो रहा है। स्कूल सहयोग करने के बजाय प्रतिस्पर्द्धा करते हैं और अक्सर मुट्ठी भर संस्थानों तक सफल मॉडल सिमटकर रह जाता है। मगर कई निजी स्कूलों ने बहुभाषी शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम और वैश्विक संपर्क की शुरुआत भी की है, जिससे छात्रों को एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली टेक कंपनियों के सहयोग से कक्षाओं को ज्यादा आकर्षक, व्यक्तिगत और भविष्यपरक बनाया गया है। हालांकि, ये लाभ भी समान रूप से सबको उपलब्ध नहीं हैं, मुख्य रूप से शहरी और महंगे स्कूल ही ऐसी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। ऐसे में, उद्देश्य और जिम्मेदारी को परिभाषित करने, विश्वास को मजबूत बनाने और डाटा-आधारित सरकारी-निजी सहयोग को आगे बढ़ाने की रणनीति खासा महत्वपूर्ण बन जाती है।
सरकारें अक्सर दीर्घकालिक ढांचागत सुधार को प्राथमिकता नहीं देतीं। निजी स्कूलों को यहीं पर आगे आना चाहिए। उनको न सिर्फ अपना संस्थान बेहतर बनाना चाहिए, बल्कि व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भी मदद करनी चाहिए। बेशक, वे सामाजिक उद्यम के रूप में संचालित होती हैं, पर ज्यादातर स्कूलों के पास बदलाव लाने के लिए जरूरी संसाधन मौजूद हैं। उन्हें आर्थिक हितों से परे जाकर जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करना चाहिए।
इसी तरह, तमाम योगदानों के बावजूद निजी स्कूलों को संदेह की नजर से देखा जाता है। यह नजरिया, जो कई मामलों में सही भी है, उन्हें फायदे के आधार पर चलने वाली संस्था के रूप में पेश करता है। इतिहास हमें यह बताता है कि निजी पहल ने अनेक क्षेत्रों में नवाचार को आगे बढ़ाया है। ऐसे में, स्कूली तंत्र को भला क्यों अपवाद बनाकर रखा जाए? हमें राज्य, निजी स्कूलों और एड-टेक कंपनियों में सामंजस्य के तरीके भी बदलने होंगे। हमें प्रदर्शन और सामूहिक जवाबदेही पर आधारित साझेदारी की जरूरत है। राज्य ऐसे मॉडल बना सकते हैं, पर निजी स्कूलों को भी सीखने की समझ बढ़ाने, योग्यता-आधारित शिक्षा पर जोर देने और रोजगार संबंधी क्षमता पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एआई का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
जाहिर है, हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो स्कूली शिक्षा को फिर से परिभाषित करना होगा। इसमें निजी स्कूलों की भूमिका नवाचार, डाटा आधारित फैसले लेने और व्यापक परिवर्तन के केंद्र की होनी चाहिए।
हेमंत जोशी
(साथ में शोधकर्ता सौभाग्य रायजादा)
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA